संबंधित पाठ्यक्रम:
सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।
संदर्भ: ICIMOD की हालिया रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र अपनी विशाल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का मात्र 6.1% ही उपयोग कर पा रहा है। विशेष रूप से, क्षेत्र में जल विद्युत जैसे संसाधनों का दोहन अभी भी अपेक्षा से कम हो रहा है।
रिपोर्ट के बारे में
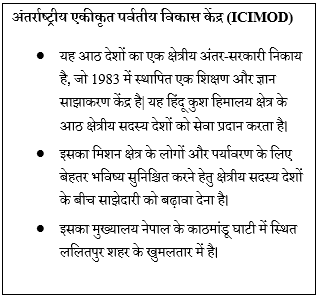
• ICIMOD ने सितंबर 2025 में ‘साथ मिलकर हमारे पास अधिक शक्ति है: हिंदू कुश हिमालय में क्षेत्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग की स्थिति, चुनौतियाँ और संभावनाएँ’ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की।
• रिपोर्ट में मौजूदा ऊर्जा स्रोतों, समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी, ऊर्जा क्षेत्र के लिए जलवायु और गैर-जलवायु जोखिमों का विश्लेषण और नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया गया है।
• हिंदूकुश हिमालय में आठ देश शामिल हैं: अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
• जलविद्युत क्षमता बनाम दोहन: हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में यानी आठ देशों में 882 गीगावाट जलविद्युत क्षमता है, जिसमें से 635 गीगावाट सीमा पार की नदियों से प्राप्त होती है। वर्तमान में इसका केवल 49% ही उपयोग में लाया जा रहा है।
• गैर-जल स्वच्छ ऊर्जा: इसमें सौर और पवन ऊर्जा शामिल है, जो हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में 3 टेरावाट के बराबर है।
• प्रतिज्ञा और क्षमता: राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुसार, हिंदूकुश हिमालय के देशों का कुल संयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 1.7 टेरावाट है; अकेले हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 3.5 टेरावाट से अधिक है।
• नवीकरणीय स्वामित्व में असमानताएं: भूटान और नेपाल अपनी सम्पूर्ण बिजली नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न करते हैं, जबकि पड़ोसी देशों अर्थात् बांग्लादेश (98%), भारत (77%), पाकिस्तान (76%), चीन (67%), और म्यांमार (51%) में बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी अधिक है।
• पारंपरिक बायोमास पर अत्यधिक निर्भरता: चार हिंदूकुश हिमालयी देशों, नेपाल (66.7%), म्यांमार (50%), भूटान और पाकिस्तान (25-25%) में जैव ईंधन और अपशिष्ट कुल प्राथमिक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं, जो लकड़ी, फसल अवशिष्ट और गोबर पर निरंतर निर्भरता पर जोर देता है, और स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
नवीकरणीय ऊर्जा की प्रगति में बाधाएँ
• वित्तीय और निवेश चुनौतियां: इस क्षेत्र को उच्च पूंजीगत लागत, सीमित सार्वजनिक वित्त, निजी निवेश को आकर्षित करने में कठिनाई और अनुसंधान एवं विकास में निरंतर निवेश की आवश्यकता जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उदाहरण: अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत में खानाबाद-2 जलविद्युत परियोजना धन और विदेशी निवेश की कमी के कारण रुकी हुई है।
• सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताएँ: स्थानीय समुदायों, पारिस्थितिकी तंत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं।
उदाहरण: भागीरथी नदी पर बने टिहरी बांध के कारण लगभग 100,000 लोग विस्थापित हो गए और 125 गांव जलमग्न हो गए, जिससे हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न हुआ।
• तकनीकी और परिचालन संबंधी चुनौतियाँ: उन्नत प्रौद्योगिकी और अनुभव की कमी, साथ ही परिचालन और रखरखाव पर सीमित जानकारी, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन और दीर्घकालिक प्रबंधन में बाधा उत्पन्न करती है।
उदाहरण: नेपाल की खसकुस्मा जलविद्युत परियोजना विशेषज्ञता की कमी, पर्याप्त तकनीकी जानकारी न होने और रखरखाव क्षमता के अभाव के कारण रुकी हुई है।
• भूमि संबंधी एवं नीतिगत चुनौतियाँ: भूमि की उपलब्धता, वायु एवं जल प्रदूषण संबंधी विचार, तथा सुदृढ़ नीति एवं नियामक ढाँचे का अभाव नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन को और जटिल बना देता है।
उदाहरण: खड़ी ढलानें, सौर ऊर्जा फार्मों के इनस्टॉलेशन में बाधा बनती हैं, तथा अकुशल नियमन के कारण जल विद्युत से जल प्रदूषण का खतरा रहता है।
• जलवायु जोखिम: इस क्षेत्र की सुभेद्य जलवायु, हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF), नदी के प्रवाह में बदलाव और चरम मौसम जल विद्युत के लिए खतरा है।
उदाहरण: सिक्किम में 2023 तीस्ता III बांध GLOF से बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और हजारों लोग विस्थापित हुए।
बाधाओं को दूर करने के लिए रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें
• क्षेत्रीय सहयोग: यह नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देता है, आपदा जोखिमों को कम करता है, कृषि व्यापार और औद्योगिक विकास को बल प्रदान करता है और कौशल एवं प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान के लिए सार्क ऊर्जा केंद्र और बिम्सटेक जैसे मंचों का लाभ उठाता है।
• निजी निवेश को प्रोत्साहित करना: यह हरित विकास और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देते हुए प्रौद्योगिकी और ज्ञान हस्तांतरण को सुगम बनाता है।
• ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना: कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है और देशों को उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करता है।

