सावलकोट जलविद्युत परियोजना
संदर्भ:
हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने जम्मू और कश्मीर में सावलकोट जलविद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की।
अन्य संबंधित जानकारी
- सावलकोट जलविद्युत परियोजना एक नदी-आधारित योजना है जिसमें जम्मू और कश्मीर के रामबन, रियासी और उधमपुर जिलों से होकर बहने वाली चिनाब नदी के पानी का उपयोग किया जाएगा।
- यह परियोजना NHPC लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, इसकी कुल स्थापित क्षमता 1,856 मेगावाट होगी और इससे प्रतिवर्ष लगभग 8,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- इस परियोजना को पहले जुलाई 2025 में चरण-I वन मंजूरी प्राप्त हुई थी और अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) द्वारा इसके मूल्यांकन के बाद इसे पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है।
- मुद्रास्फीति और प्रशासनिक देरी के कारण परियोजना की अनुमानित लागत ₹22,000 करोड़ से बढ़कर ₹31,380 करोड़ हो गई है।
सावलकोट जलविद्युत परियोजना की मुख्य विशेषताएं
- परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 1,856 मेगावाट है, जिसमें चरण 1 (1,406 मेगावाट) में 225 मेगावाट की छह इकाइयाँ और 56 मेगावाट की एक इकाई और चरण 2 (450 मेगावाट) में 225 मेगावाट की दो इकाइयाँ शामिल हैं।
- परियोजना का विकास ₹31,380 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जाएगा, जिसमें कुल 1,401.35 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल होगा, जिसमें 17 हेक्टेयर वन भूमि और 554.18 हेक्टेयर गैर-वन भूमि शामिल है।
- इस परियोजना में 5 मीटर ऊंचे RCC गुरुत्व बांध का निर्माण शामिल होगा, जिससे यह सिंधु बेसिन की पूर्वी सहायक नदियों पर सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक बन जाएगी।
- इस परियोजना से प्रतिवर्ष 8,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने परियोजना को मंज़ूरी दे दी है और इसके चालू होने के पाँच साल बाद एक स्वतंत्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की सिफ़ारिश की है।
- यह परियोजना किसी भी अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है और इसकी जन सुनवाई जम्मू और कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2016 में की गई थी।
मिशन दृष्टि
संदर्भ:
गैलेक्सआई (बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप) उन्नत इमेजिंग क्षमताओं से लैस विश्व का पहला मल्टी-सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी में है।
अन्य संबंधित जानकारी
- यह मिशन दृष्टि 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा, जो गैलेक्सआई के उपग्रह तारामंडल कार्यक्रम की शुरुआत को चिह्नित करेगा। इसका उद्देश्य 2029 तक रियल टाइम पृथ्वी अवलोकन क्षमता हासिल करना है।
- यह मिशन सरकारों, रक्षा एजेंसियों और उद्योगों को सीमा की निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि निगरानी, बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन और रक्षा संचालन जैसे अनुप्रयोगों के लिए उन्नत भू-स्थानिक विश्लेषण करने में सक्षम बनाएगा।
- यह कंपनी अगले चार वर्षों में आठ से बारह उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की योजना बना रही है, जिससे सभी मौसमों और दिन-रात पृथ्वी का अवलोकन करने में सक्षम एक तारामंडल का निर्माण होगा।
- यह मिशन वाणिज्यिक, रणनीतिक और पर्यावरणीय अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी, उच्च आवृत्ति और सटीक पृथ्वी अवलोकन डेटा प्रदान करके भारत को वैश्विक अंतरिक्ष नवाचार मानचित्र में उच्च प्रतिष्ठा दिलाएगा।
दृष्टि मिशन की विशेषताएँ
- मिशन दृष्टि, दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जो सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) और मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग (MSI) सेंसर को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा।
- सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) एक सुदूर संवेदन तकनीक है जो किसी भी मौसम या अवधि में पृथ्वी की सतह की उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां बनाने के लिए रडार पल्स का उपयोग करती है।
- मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग (MSI) एक ऐसी तकनीक है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की कई, विशिष्ट तरंग दैर्ध्य श्रेणियों में छवियों को कैप्चर करती है और उनका विश्लेषण करती है।
- यह उपग्रह गैलेक्सआई की स्वामित्व वाली सिंकफ्यूज्ड ऑप्टो-एसएआर तकनीक से लैस है, जो व्यापक और बादल-स्वतंत्र पृथ्वी अवलोकन डेटा प्रदान करने के लिए रडार और ऑप्टिकल इमेजरी को एकीकृत करता है।
- इस उपग्रह का वजन 160 किलोग्राम है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम-रिज़ॉल्यूशन वाला उपग्रह बनाता है।
- यह मिशन 5 मीटर रिज़ॉल्यूशन पर एकीकृत, विश्लेषण-तैयार इमेजरी प्रदान करता है और इसे गति, विश्वसनीयता और एआई-तैयारी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो रक्षा, आपदा प्रबंधन और कृषि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है।
अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन
संदर्भ:
हाल ही में, महाराष्ट्र के पांच समुद्र तटों को स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
अन्य संबंधित जानकारी
- प्रमाणन प्राप्त करने वाले समुद्र तटों में रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन और नागांव समुद्र तट, पालघर जिले के परनाका समुद्र तट, तथा रत्नागिरी जिले के गुहागर और लाडघर समुद्र तट शामिल हैं।
- इस मान्यता के बाद महाराष्ट्र पर्यावरण अनुकूल तटीय प्रबंधन और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने वाले राज्यों में शामिल हो गया है।
- यह प्रमाणन डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE) द्वारा प्रदान किया गया है जो वैश्विक ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की देखरेख करता है।
- भारत में अब कुल 18 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं।
ब्लू फ्लैग प्रमाणन
- ब्लू फ्लैग कार्यक्रम 1985 में फ्रांस में शुरू हुआ।
- यह पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित है और इसका मुख्यालय कोपेनहेगन, डेनमार्क में है।
- यह प्रमाणन उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो पर्यावरण, शैक्षिक, सुरक्षा और सुगम्यता के 33 मानदंडों को पूरा करते हैं।
- प्रमाणन के लिए चार प्रमुख श्रेणियां हैं:
- जल गुणवत्ता
- पर्यावरण प्रबंधन
- पर्यावरण शिक्षा
- सुरक्षा
- पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन (FEE) विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको-लेबल – ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान करता है।
- FEE यह सुनिश्चित करता है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन के उच्च मानकों को विश्व भर में निरंतर बनाए रखा जाए।
- इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु, पर्यावरण, शैक्षिक, सुरक्षा-संबंधी और पहुँच-संबंधी कई सख्त मानदंडों को पूरा करना और उन्हें बनाए रखना अनिवार्य है।
- ब्लू फ्लैग का मिशन पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य सतत विकास अभ्यासों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है।
मसालों और पाककला जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति का 8वाँ सत्र
संदर्भ:
भारत ने मसाला गुणवत्ता, सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार के लिए वैश्विक मानकों को सुदृढ़ करने हेतु गुवाहाटी, असम में मसालों और पाककला जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) के 8वें सत्र की मेजबानी की।
अन्य संबंधित जानकारी
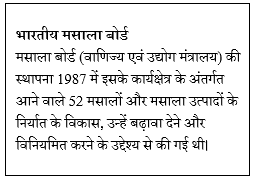
- गुवाहाटी सत्र का उद्देश्य वैश्विक मसाला मानक स्थापित करने, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और मसाला उद्योग में सतत विकास सुनिश्चित करने में भारत के नेतृत्व की पुष्टि करना है।
- इस सत्र की मेजबानी भारत सरकार द्वारा की जा रही है, जिसमें भारतीय मसाला बोर्ड, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (CAC) के तहत सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग सुरक्षित और निष्पक्ष खाद्य व्यापार पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व व्यापार संगठन के तहत संयुक्त रूप से कार्य करता है।
- राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि CCSCH विज्ञान आधारित और वैश्विक दृष्टि से सुसंगत मानकों के माध्यम से भारत की विविध मसाला जैव विविधता को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मसालों और पाककला संबंधी जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH)
- समिति की स्थापना 2013 में कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (CAC) के अंतर्गत एक कमोडिटी समित्ति के रूप में की गई थी।
- भारत शुरू से ही इस प्रतिष्ठित समिति की मेजबानी करता रहा है और भारतीय मसाला बोर्ड इसके सचिवालय संगठन के रूप में कार्य करता है तथा समिति के सत्रों का आयोजन करता है।
- मसालों और पाककला संबंधी जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) की अध्यक्षता भारत करता है और यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के अधीन कार्य करती है।
- CCSCH का सचिवालय कोच्चि, केरल में है।
- अपनी स्थापना के बाद से, CCSCH ने 16 मसालों के लिए 14 अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित किए हैं, जिससे वैश्विक मसाला मानकीकरण में भारत के नेतृत्व को मजबूती मिली है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग को खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में मान्यता देता है।
भारत-दक्षिण कोरिया का प्रथम द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास
संदर्भ:
हाल ही में, दक्षिण कोरिया ने बुसान में पहली बार भारत-कोरिया गणराज्य नौसेना (IN-RoKN) द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की, जो समुद्री सहयोग में एक नए चरण का प्रतीक है।
अन्य संबंधित जानकारी
- भारत-कोरिया गणराज्य नौसेना (IN-RoKN) द्विपक्षीय अभ्यास का उद्घाटन 13 अक्टूबर, 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान नौसेना बेस पर हुआ।
- भारत में निर्मित शिवालिक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट INS सह्याद्रि ने इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- कोरिया गणराज्य की नौसेना (RoKN) ने भारतीय युद्धपोत का औपचारिक स्वागत किया, जो दोनों नौसेनाओं के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों का प्रतीक है।
- यह आयोजन भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के तहत दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच नियमित द्विपक्षीय संबंधों के संस्थागतरण का प्रतीक है।
- इस अभ्यास में दो चरण शामिल हैं – एक बंदरगाह चरण और दूसरा समुद्री चरण – जिनका उद्देश्य परिचालन तालमेल और आपसी समझ में सुधार करना है।
बंदरगाह चरण
- बंदरगाह चरण में परिचालन संबंधी ज्ञान और सर्वोत्तम अभ्यासों का आदान-प्रदान करने के लिए नौसेना कर्मियों द्वारा क्रॉस-डेक दौरे शामिल होते हैं।
- दोनों पक्षों के अधिकारियों ने समुद्री रणनीति, समुद्री डकैती रोधी उपायों और मानवीय सहायता पर केंद्रित चर्चा में भाग लिया।
समुद्री चरण
- समुद्री चरण में INS सह्याद्रि और ROKS ग्योंगनाम (ROK नौसेना का डेगू-क्लास फ्रिगेट) के बीच संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ।
- दोनों जहाज सामरिक समन्वय में सुधार के लिए समुद्री अवरोधन अभियान (MIOs) और पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) अभ्यास किया।
अभ्यास का महत्व
- यह अभ्यास स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- यह भारत की बढ़ती समुद्री पहुँच और क्षेत्र में एक पसंदीदा सुरक्षा साझेदार के रूप में उसकी भूमिका को रेखांकित करता है।
सरकार ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया
संदर्भ:
हाल ही में, केन्द्रीय खान मंत्रालय ने चूना पत्थर के सभी रूपों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है।
अन्य संबंधित जानकारी
- मंत्रालय ने पट्टों के सुचारू हस्तांतरण के लिए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 20A के अंतर्गत एक आदेश जारी किया।
- यह आदेश सुनिश्चित करता है कि मौजूदा गौण खनिज चूना पत्थर पट्टे बिना किसी व्यवधान के प्रमुख खनिज पट्टों के रूप में कार्य करते रहेंगे।
- इस निर्णय के बाद से पूर्व में किया गया दोहरा वर्गीकरण समाप्त हो जाएगा, जिसके तहत चूना पत्थर को निर्माण सामग्री के लिए चूना भट्टों में उपयोग किए जाने पर गौण खनिज जबकि सीमेंट, इस्पात या रासायनिक उद्योगों में उपयोग किए जाने पर प्रमुख खनिज माना जाता था।
- यह सुधार पट्टाधारकों को अंतिम उपयोग के आधार पर बिना प्रतिबंधों के किसी भी औद्योगिक उद्देश्य के लिए चूना पत्थर बेचने या उपयोग करने की अनुमति देता है।
- इस कदम का उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, व्यावसायिक परिस्थितियों में सुधार लाना और खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण रोजगार का विस्तार करना है।
- यह निर्णय नीति आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में गठित अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के उपरांत, विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद लिया गया है।
नियामक संक्रमण उपाय
- मौजूदा पट्टाधारकों को 31 मार्च, 2026 तक भारतीय खान ब्यूरो (IBM) में पंजीकरण कराना होगा और उस तिथि तक राज्य सरकार की मौजूदा दरों पर रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।
- राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित मौजूदा खनन योजनाएँ 31 मार्च, 2027 तक वैध रहेंगी और पट्टाधारकों को इस अवधि के भीतर खनन योजनाओं के लिए IBM की मंज़ूरी लेनी होगी।
- यह आदेश 1 जुलाई, 2027 तक पट्टा क्षेत्रों की डिजिटल हवाई तस्वीरें जमा करने से और 31 मार्च, 2026 तक IBM को मासिक और वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने पर लगने वाले जुर्माने से अस्थायी छूट प्रदान करता है।
- हालाँकि, पट्टाधारकों को मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अपनी-अपनी राज्य सरकारों को रिटर्न प्रस्तुत करना जारी रखना होगा।
वर्गीकरण का आर्थिक प्रभाव
- व्यापार सुगमता (EoDB)- पट्टाधारक गौण या प्रमुख खनिज के कृत्रिम नियामक भेद के आधार पर उनके अंतिम उपयोग पर प्रतिबंध लगाए बिना किसी भी उद्देश्य के लिए चूना पत्थर बेच या उपयोग कर सकेंगे।
- आर्थिक अवसर – इस सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि खनिकों और श्रमिकों को उच्च माँग और व्यापक बाजार पहुँच का लाभ मिलेगा।
- निर्माण आधारित उद्योगों को बढ़ावा – सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे देश में सीमेंट निर्माण क्षमता का तेजी से विस्तार हो सकेगा।
अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025
संदर्भ:
निवारक और समुदाय-नेतृत्व वाली जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है।
अन्य संबंधित जानकारी
- 2025 का विषय, “आपदाओं में नहीं, आपदा-रोधन में निवेश करें” आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए वित्तपोषण बढ़ाने पर जोर देता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी विकास और निजी निवेशों के जोखिम के बारे में पता हो और उनसे निपटने के लिए स्थिति अनुरूप उपाय किए जाएं।
- वर्ष 2025 में यह दिवस वैश्विक व्यय प्राथमिकताओं को आपदा-पश्चात प्रतिक्रिया से हटाकर निवारक उपायों, स्थानीय लचीलेपन और टिकाऊ बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- इस वर्ष के अभियान में सरकारों से सार्वजनिक और अंतर्राष्ट्रीय बजट दोनों में DRR के लिए वित्त पोषण बढ़ाने का आग्रह किया गया है।
- इस दिवस की घोषणा पहली बार 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा की गई थी, ताकि प्रत्येक नागरिक और सरकार को आपदा की तैयारी और रोकथाम में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
वैश्विक चिंताएँ
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक आकलन रिपोर्ट, 2025 में अनुमान लगाया गया है कि सालाना 202 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष वैश्विक नुकसान होगा, जबकि वास्तविक लागत लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर होगी।
- दुनिया भर में सार्वजनिक बजट का 1% से भी कम हिस्सा आपदा न्यूनीकरण (DRR) के लिए दिया जाता है, और 2019 और 2023 के बीच केवल 2% आधिकारिक विकास सहायता (ODA) परियोजनाओं में DRR लक्ष्य शामिल थे।
2025 में भारत का अनुभव
- भारत में 2025 में केवल आठ महीनों के दौरान आपदाओं से 3,502 मौतें हुईं और 235 चरम मौसम के दिवस दर्ज किए गए, जो 2022 से इनमें हुई तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।
- ये आपदाएँ जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा पैटर्न, कुप्रबंधित बाँधों और अनियोजित शहरी एवं तटीय विकास के कारण हुईं।
- छह वर्षों में बिजली गिरने की घटनाओं में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे अप्रैल और जुलाई 2025 के बीच 1,600 से अधिक लोगों की मौत हुई है।
विश्व सांख्यिकी दिवस 2025
संदर्भ:
सतत विकास के लिए विश्वसनीय आंकड़ों को बढ़ावा देने हेतु विश्वभर में 20 अक्टूबर को चौथा ‘विश्व सांख्यिकी दिवस’ मनाया जाएगा।
अन्य संबंधित जानकारी
- 2025 का विषय, “सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डेटा“, समाज के हर स्तर पर निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय और सुलभ डेटा की आवश्यकता पर केंद्रित है।
- यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जाएगा, जो वैश्विक प्रगति को आगे बढ़ाने में विश्वसनीय और समावेशी डेटा प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
- यह दिवस वैश्विक सांख्यिकीय समुदाय की उपलब्धियों का प्रतीक है, जो सहयोग को बढ़ावा देता है, मानक विकसित करता है तथा सटीक, समय पर और नैतिक डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- यह दिवस इस बात की पुष्टि करता है कि जलवायु परिवर्तन, शांति स्थापना, सतत विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए सांख्यिकी आवश्यक है।
- भारत में सांख्यिकीविदों द्वारा दिए गए असाधारण योगदान के महत्त्व को रेखांकित करने और उसकी सराहना करने के लिए, विशेष रूप से प्रख्यात सांख्यिकीविद् (दिवंगत) प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में, प्रति वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है।

