संबंधित पाठ्यक्रम
सामान्य अध्ययन-2: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली।
संदर्भ: विधि एवं न्याय मंत्री ने वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution -ADR) तंत्र को मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के बारे में
• ADR उन तंत्रों को संदर्भित करता है जो पारंपरिक अदालतों के बाहर विवादों का निपटारा करते हैं।
• इसमें कुशलतापूर्वक और गोपनीय तरीके से आपसी समझौतों तक पहुँचने के लिए तटस्थ सुविधा या प्रत्यक्ष संवाद शामिल है।
• ADR के तंत्र:
- मध्यस्थता (Mediation): एक तटस्थ मध्यस्थ विवादित पक्षों को मुद्दों पर चर्चा करने और स्वैच्छिक समझौते तक पहुंचने में मदद करता है, लेकिन मध्यस्थ कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं लेता है।
- माध्यस्थम् (Arbitration): दोनों पक्ष अपना मामला मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो फिर सामान्यतः बाध्यकारी और प्रवर्तनीय निर्णय देता है।
- वार्ता (Negotiation): दोनों पक्ष, किसी तटस्थ तीसरे पक्ष को शामिल किए बिना अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रत्यक्ष चर्चा में संलग्न होते हैं।
- सुलह (Conciliation): एक अनौपचारिक, स्वैच्छिक विवाद समाधान जहाँ एक तटस्थ सुलहकार दोनों पक्षों को आपसी संवाद करने में मदद करता है और गैर-बाध्यकारी समाधान सुझा सकता है।
- तटस्थ मूल्यांकन (Neutral Evaluation): यदि मामला अदालत में जाता है तो एक तटस्थ तृतीय पक्ष मामले के संभावित परिणाम पर अपनी राय प्रदान करता है।
- न्यायिक निपटान/लोक अदालत: औपचारिक न्यायालय प्रणाली के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए भारत में स्थापित एक तंत्र।
वैकल्पिक विवाद समाधान का संवैधानिक और कानूनी आधार
• संवैधानिक आधार:
- अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21: ADR अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) पर आधारित है, जो सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष और समय पर न्याय सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 39A: यह राज्य को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, जिससे ADR कमजोर वर्ग के लिए न्याय की गारंटी का साधन बन सके।
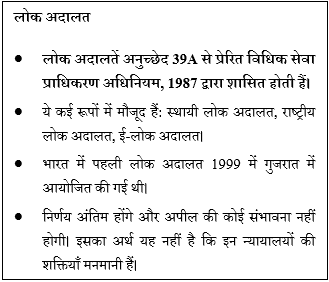
• कानूनी आधार:
- माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996: माध्यस्थम् और सुलह को विनियमित करने वाला प्राथमिक क़ानून, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विवादों को कवर करता है।
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: धारा 89 अदालतों को मध्यस्थता, विवाद निपटान, सुलह या लोक अदालत सहित वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए मामलों को संदर्भित करने का अधिकार देती है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987: ADR तंत्र सहित लोक अदालतों और कानूनी सहायता के लिए रूपरेखा स्थापित करता है।
- मध्यस्थता अधिनियम 2023: भारत में संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक औपचारिक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, जो मध्यस्थों की नियुक्ति, मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन और मध्यस्थता से किए गए निपटान समझौतों की प्रवर्तनीयता को नियंत्रित करता है।
ADR का महत्त्व
• तंत्र की अक्षमताओं को दूर करना:
- मामलों का लंबित रहना (Pendency of cases): राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, भारत में कुल लंबित मामले 4,57,96,239 है; सर्वोच्च न्यायालय में 81,768 और उच्च न्यायालयों में लगभग 62.9 लाख मामले लंबित हैं।
- उच्च रिक्ति दर: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बताया गया है कि उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में क्रमशः 33% और 21% रिक्ति दर है।
- न्यायिक कार्यभार: उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में न्यायाधीशों पर 4,000 से अधिक मामलों का कार्यभार है।
• सामाजिक और प्रक्रियात्मक लाभ:
- सामाजिक परिवर्तन उत्प्रेरक: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, मध्यस्थता को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन मानते हैं, जो संवाद और सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को संवैधानिक मूल्यों के साथ संरेखित करता है।
- लचीलापन और पक्ष नियंत्रण: ADR में पक्षों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, जिसमें निर्णयकर्ताओं का चयन करना, लागू कानूनों का चयन करना और प्रक्रिया के नियमों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शामिल है।
- सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक समाधान: ADR पक्षों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप रचनात्मक और संतोषजनक परिणाम देता है, जिससे अधिक स्थायी समाधान मिलते हैं।

